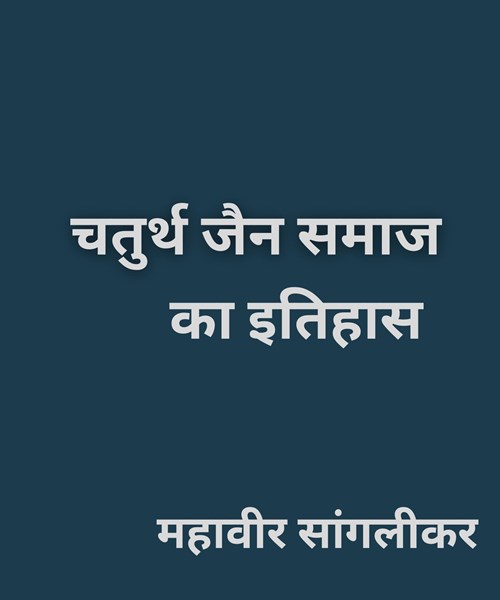संजय सोनवणी, पुणे
“जिन” शब्द का अर्थ है—जो अपने भीतर के विकारों पर विजय पा ले. यही अर्थ योग की मूल भावना की ओर संकेत करता है. जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ ही योग के प्रवर्तक थे, जिसे उस समय व्रत कहा जाता था. माना जाता है कि भगवान ऋषभनाथ का जीवनकाल लगभग 3000 से 2700 ईसा पूर्व के बीच था और उन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व माना जाता है.
अन्य समकालीन स्रोतों के अभाव में यह कहना उचित है कि श्रमण परंपरा की शुरुआत ऋषभनाथ से ही हुई. आगे चलकर यही परंपरा कई दार्शनिक धाराओं और संप्रदायों में विभाजित हुई, जिनकी अपनी-अपनी मान्यताएं बनीं.
व्रत, व्रात्य और योग की प्रारंभिक परंपरा
प्रारंभ में अधिकांश दार्शनिक समूहों ने “योग” शब्द को स्वीकार नहीं किया था. इसका मूल शब्द व्रत था, जिसका अर्थ है संयमित प्रतिज्ञाएं. जो लोग इन व्रतों का कठोरता से पालन करते थे, उन्हें व्रात्य कहा जाता था. वर्णनों से पता चलता है कि व्रात्य ऐसे संन्यासी थे जिन्होंने व्रतों के कारण सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था.
जैन धर्म के मूल व्रत हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (असंग्रह). यही व्रत आज के योग की नींव हैं, क्योंकि इनमें मानव प्रवृत्तियों पर नियंत्रण आवश्यक है. पतंजलि ने भी अपने योगसूत्र में इन पांच जैन व्रतों को यम (नैतिक नियम) के रूप में स्वीकार किया है.
समय के साथ “व्रात्य” शब्द प्रचलन से बाहर होता गया, क्योंकि वैदिक श्रेष्ठतावादियों ने उन विचारों का श्रेय लेने का प्रयास किया जिन्हें उन्होंने स्वयं विकसित नहीं किया था. ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी तक “योग” शब्द अधिक लोकप्रिय हो गया, पर उसका आधार अब भी व्रत ही था.
वास्तव में पतंजलि ने योग के पहले अंग के रूप में यम को बताया है, जो मूलतः व्रत ही हैं. दूसरा अंग नियम है, जो व्रतों को सहारा देने वाले अनुशासन हैं. इसके बाद आसन आते हैं, अर्थात शारीरिक मुद्राएं.
भगवती सूत्र और महावीर की योग-साधना
जैन आगमों में पांचवें स्थान पर आने वाला भगवती सूत्र भगवान महावीर के उपदेशों को समेटे हुए है. इसे 466 ईस्वी में वल्लभी में हुई अंतिम जैन परिषद में लिपिबद्ध किया गया था. इससे पहले ये उपदेश मौखिक परंपरा से चले आ रहे थे. इस सूत्र में भगवान महावीर सोमिल को बताते हैं कि उनका जीवन-मार्ग छह साधनाओं से बना है:
तप (तपस्या), नियम (अनुशासन), संयम (आत्म-नियंत्रण), स्वाध्याय (आत्म-अध्ययन), ध्यान (ध्यान-योग), आवश्यकीय (सचेत रूप से आवश्यक कर्तव्यों का पालन)
(स्रोत: भगवती सूत्र, खंड 1, अनुवाद—के. सी. लालवानी, जैन भवन, कोलकाता, 1999)
जैन धर्म में योग की धारणा
योगसूत्र में पतंजलि यम और नियम जैसे सिद्धांतों की चर्चा करते हैं. उदाहरण के लिए, “शौच” को जैन परंपरा में मानसिक पवित्रता माना गया है, जबकि पतंजलि ने शारीरिक स्वच्छता पर अधिक ज़ोर दिया है. जैन धर्म में आसन को भी योग का अंग माना गया है, विशेष रूप से कायक्लेश तप और बाह्य तपस्या के रूप में. वहीं पतंजलि के अनुसार आसन आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन हैं.
योगसूत्र विभिन्न दृष्टिकोणों से योग के अंगों का विस्तार करता है. कुल मिलाकर यह ग्रंथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन या श्रमण ध्यान-पद्धतियों का ही विस्तार है.
योग प्रणाली की उत्पत्ति श्रमणों या जैनों से जुड़ी हुई है—यह बात जैन ग्रंथों में इसके क्रमिक विकास से स्पष्ट होती है. जैन योग मुक्ति के लिए चार चरणों पर आधारित है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप
बाद की परंपराओं ने इन्हें भले ही अलग नामों से अपनाया हो, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहे.
जैनों और श्रमण आंदोलन के आचार्यों के लिए प्रारंभ में योग का अर्थ ही व्रत था. व्रत, जिसमें विशेष साधनाएं आवश्यक थीं, संभवतः योग का सबसे प्रारंभिक नाम था और आगे चलकर पतंजलि ने इसी आधार पर योग दर्शन का विस्तार किया. प्रारंभिक वैदिक आर्यों द्वारा जिन व्रात्यों का उल्लेख मिलता है, वे अपने समय के योगी ही थे, जो एक नई अनुशासन-पद्धति का अभ्यास करते थे.
व्रत हमेशा आत्मबोध और मुक्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास था. यह किसी बाहरी सर्वोच्च सत्ता से जुड़ने की प्रक्रिया नहीं थी. प्रारंभिक जैन दर्शन में योग उस प्रक्रिया को कहा गया जिसमें कर्मों के आवेग आत्मा से चिपक जाते हैं और उसकी वास्तविक चमक को ढक देते हैं.
उपनिषद और श्रमण प्रभाव
क्रिस्टोफर की चैपल के अनुसार “संस्कृति में इस शब्द के प्रयोग में आए परिवर्तन, जो संभवतः उत्तर उपनिषद काल में हुए, उनके प्रत्युत्तर में जैन विचारकों ने अपनी धार्मिक साधना को योग की नई परिभाषाओं के संदर्भ में समझाना शुरू किया, जहां योग का अर्थ मानसिक शांति प्राप्त करने की तकनीकों से जोड़ा गया.”
(योग इन जैनिज़्म, संपादक—क्रिस्टोफर की चैपल, रूटलेज, 2016, पृष्ठ 10)
इसका अर्थ यह है कि समय के साथ शब्दावली बदली, पर मूल भावना वही रही. यही कारण है कि उपनिषदों पर श्रमण परंपरा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, भले ही वैदिक प्रभाव के कारण वहां अलग शब्दों का प्रयोग हुआ हो.
समभाव ही व्रत या योग की आधारशिला है और यही श्रमण परंपरा का सार है. प्राकृत भाषा में “श्रमण” का अर्थ है—जो सभी को समान दृष्टि से देखे.
भगवती आराधना (गाथा 70, विजयादया टीका) के अनुसार—
“समणो” अर्थात “समानस्य भावः समनं”
अर्थात श्रमण वह है जिसमें समानता का भाव हो.
इससे स्पष्ट होता है कि श्रमण का अर्थ है—समान दृष्टि और संतुलित भाव. “समण्ण” ऐसी दृष्टि को दर्शाता है जिसमें कोई द्वेष नहीं होता. हरगोविंद सेठ के प्राकृत शब्दकोश में भी श्रमण की परिभाषा है—“जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखे.”
++++
लेखक परिचय
संजय सोनावणी भारत के एक शोधकर्ता हैं, जो दर्शन, धर्म, विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, भाषा-विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि अनेक क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं. वे 130 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं और उनके हजारों लेख प्रिंट व ऑनलाइन माध्यमों में प्रकाशित हो चुके हैं.
यह भी पढिये …..
Jains & Jainism (Online Jain Magazine)
They Won Hindi (हिंदी कहानियां व लेख)
TheyWon
English Short Stories & Articles